पृथ्वी पर जीवन को कायम रखने में अनेक तत्त्वों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है. लेकिन इन सभी तत्त्वों का आधार ऊर्जा ही है और पृथ्वी पर ऊर्जा के अधिकांश भाग का मूल स्रोत सूर्य ही है. सूर्य एक विशाल गैसीय पिंड है. सूर्य का तापमान काफी अधिक होता है इसलिए इस पर कोई पदार्थ ठोस या तरल स्थिति में नहीं है. यहां पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था उपस्थित है. 21 जून, 2020 को हमारा यह सूर्य चंद्रमा के द्वारा पूरा ढँक लिया जाएगा और उस समय अद्भुत नजारा देखा जा सकेगा. आदिकाल से ही सभी सभ्यताओं में इस घटना को लेकर उत्सुकता रही है. पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना को लेकर जनमानस में भय और अनेक मिथक भी प्रचलित होते रहे हैं. इस लेख के माध्यम से सूर्य के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है.
खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों ओर एक धुंधला सा आभामंडल दिखाई देता है. इसे सौरमंडल या सौर वायुमंडल (सोलर कोरोना) कहते हैं. सूर्य का व्यास लगभग 14,00,000 किलोमीटर है. सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान 15×10″6 केल्विन होता है. हालांकि सूर्य की सतह का तापमान अपेक्षाकृत कम (लगभग 6,000 केल्विन) होता है. सूर्य के केंद्रीय भाग का घनत्व 150 ग्राम प्रति घन सेमी. होता है. इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर इसका भार पानी की तुलना में करीब 150 गुना अधिक है. ऐसा सूर्य के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षणीय दबाव की वजह से होता है. इसी कारण सूर्य के केंद्रीय भाग का दाब, ताप एवं घनत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है. सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में करीबन 3 लाख 53 हजार गुना अधिक है. अनुमानतः सूर्य का द्रव्यमान 2×10″30 किलोग्राम है. सूर्य इतना बड़ा है कि इसको ढँकने के लिए हमारी पृथ्वी जैसी 109 और पृथ्वियों की आवश्यकता होगी.

गैसीय गोला होने के कारण सूर्य अपनी धुरी पर 25 दिन में एक चक्कर लगाता है क्योंकि सूर्य ठोस पिंड न होकर गैस का गोला है, इसलिए इसके विभिन्न भाग अलग-अलग रफ़्तार से घूमते हैं. विषुवत् रेखा पर इसकी घूर्णन अवधि 25 दिन होती है. ध्रुवीय प्रदेश की ओर बढ़ने पर यह अवधि क्रमशः बढ़ती जाती है. ध्रुवों पर यह अवधि 31 दिन होती है. सूर्य का घूर्णन क्रान्तिवृत्त के तल के साथ करीब 83 डिग्री झुका होता है. इसलिए यह धुरी क्रांतिवृत्त के तल के साथ करीब 7 डिग्री का कोण बनाती है.
सूर्य की संरचना
सूर्य एक गैसीय पिंड है. इसलिए इसकी संरचना पृथ्वी से भिन्न है. सूर्य में कोई ठोस सतह नहीं है. सूर्य में एक के बाद एक संकेंद्री गोलाकार कवच या परतें हैं. मुख्यतः सूर्य की बनावट को तीन परतों के रूप में समझा जाता है. हर परत में विशिष्ट प्रकार की भौतिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं. हालांकि सूर्य की सबसे आंतरिक परत कोर यानी केंद्र में नाभिकीय भट्टी सी अभिक्रियाएं चलती रहती हैं. सूर्य में द्रव्यमान के हिसाब से हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 94 प्रतिशत और हीलियम की मात्रा 6 प्रतिशत है. कोर में चलने वाली प्रक्रियाओं के द्वारा हाइड्रोजन के अणु हीलियम के नाभिक में परिवर्तित होते रहते हैं जिसकी दर प्रति सेकण्ड 60 करोड़ लाख टन है. इस नाभिकीय प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा विद्युतचुम्बकीय ऊर्जा के फोटॉनों के रूप में केंद्र के बाद ऊपर की ओर विकिरणी क्षेत्र में आती है. उसके बाद संवहनी क्षेत्र आता है फिर क्रमशः प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और संक्रमण क्षेत्र स्थित हैं. सूर्य के सबसे बाहरी क्षेत्र में आभामंडल यानी कोरोना स्थित होता है. हालांकि सूर्य का केंद्र ही अन्य सभी क्षेत्रों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है. केंद्र में प्रज्वलित नाभिकीय भट्ठी से ऊर्जा एक के बाद एक आने वाली बाहरी परतों में विकिरण एवं संवहन प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचती है. सूर्य के केंद्र का तापमान 15×10″6 केल्विन होता है और बाहर की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी आती जाती है. तापमान में कमी का सिलसिला वर्णमंडल आने तक चलता रहता है. वर्णमंडल में तापमान घटकर 4×10″3 केल्विन रह जाता है. ऊर्जा का प्रसार विकिरण के बजाय संवहन प्रक्रिया से उन क्षेत्रों में होता है जिनमें तापमान घट कर 2×10″6 केल्विन से कम रह जाता है. इन क्षेत्रों में विकिरण के बजाय संवहन ही ऊर्जा के प्रसार का प्रभावी माध्यम बन जाता है. ऊर्जा के प्रसार के आधार पर ही विकिरण क्षेत्र और संवहन क्षेत्र में विभेद किया जा सकता है. नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली सूर्य की सबसे अंदरूनी परत प्रकाश मंडल है जो सूर्य के मुश्किल से दिखने वाले वायुमंडल की तुलना में अधिक चमकीला होता है. आमतौर पर हम नंगी आंखों से सूर्य के प्रकाश मंडल को देखकर ही उसके आकार का अनुमान लगाते हैं. सूर्य के प्रकाश मंडल के ठीक बाहर उसकी वायुमंडलीय परत होती है. प्रकाश मंडल की तीव्रता के कारण वर्णमंडल से उत्सर्जित दृश्य किरणें विशिष्ट फिल्टर के बिना देखने पर श्याम नजर आती हैं एवं खग्रास सूर्य ग्रहण की पूर्णता की स्थिति के दौरान चंद्रमा सूरज के प्रकाशमंडल को ढक लेता है. हालांकि सूर्य ग्रहण की पूर्णता की स्थिति से ठीक पहले वर्ण मंडल को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है. उस समय यह लाल रंग की क्षणिक दीप्ति में दिखाई देता है. इस लालप्रकाश का तरंगदैर्घ्य 656 नैनोमीटर होता है. इस लाल प्रकाश का उत्सर्जन हाइड्रोजन की परमाणु संरचना में परिवर्तन के कारण होता है.
सूर्य के बाह्य वायुमंडल की संभवतः सबसे अनोखी विशेषता उसके तापमान का बेढंगा उतार-चढ़ाव है. केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ ही सूर्य के वर्णमंडल तक जिस प्रकार से तापमान में क्रमिक गिरावट आनी चाहिए वैसी नहीं आती है. वर्णमंडल तक तो तापमान में क्रमिक रूप से गिरावट आती है लेकिन संक्रमण क्षेत्र में इसमें पुनः तेजी से वृद्धि हो जाती है. इसलिए तापमान में अचानक वृद्धि होने के कारण इस क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है.
सूर्य की रासायनिक संरचना
सूर्य की रासायनिक संरचना में मुख्यतः दो तलों हाइड्रोजन और हीलियम का योगदान सर्वाधिक है. हालांकि आवर्तसारणी में ये दोनों सबसे हल्के तत्व हैं. घटते क्रम में सूर्य में ऑक्सीजन और कार्बन का बाहुल्य है. इनके अलावा भार की दृष्टि में सूर्य की रासायनिक संरचना में अन्य तत्वों का योगदान लगभग एक प्रतिशत से भी कम है. सूर्य की रासायनिक संरचना के सम्बन्ध में एक दिलचस्प बात यह है कि सूर्य पर हीलियम की उपस्थिति का पता पहले चला, धरती पर उसकी खोज बाद में की गई. सूर्य पर हीलियम की खोज 1868 ई. में हो चुकी थी जबकि पृथ्वी पर हीलियम की खोज 1895 में की जा सकी.
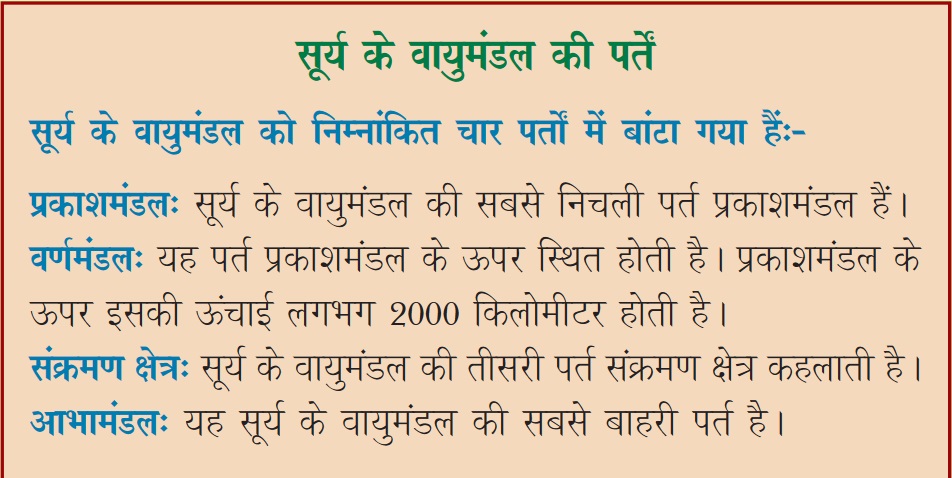
ऊर्जा का अक्षय भंडार – सौर ऊर्जा
ऊर्जा के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है. पृथ्वी पर ऊर्जा का अक्षय स्रोत सूर्य है. सूर्य लगभग पांच अरब वर्षों से चमकता आ रहा है और यह पांच अरब वर्षों तक और चमकता रहेगा. सूर्य की ऊर्जा का कारण इसमें निरन्तर चलने वाली संलयन अभिक्रिया है. सूर्य में विशाल द्रव्य राशि की उपस्थिति के कारण उसका गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव काफी बढ़ जाता है जिसके परिणामस्वरूप सूर्य के केंद्र पर अत्यधिक दवाब होता है. इस दबाव को तभी संतुलित रखा जा सकता है जब सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान काफी अधिक हो. बहुत अधिक तापमान पर हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम के नाभिकों में परिवर्तित होने लगते हैं. इस प्रक्रिया को ताप-नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं. इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के चार नाभिक आपस में मिलकर एक हीलियम बना लेते हैं. इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है. सूर्य के केंद्र में संलयन अभिक्रिया के कारण प्रति सेकंड 42.50 लाख टन हाइड्रोजन, हीलियम में परिवर्तित होती है. सूर्य के समान अन्य तारों में भी इसी प्रक्रिया से ऊर्जा पैदा होती है.
सूर्य में उपस्थित हाइड्रोजन का भण्डार हर पल कम होता जा रहा है. जब यह भण्डार समाप्त हो जाएगा तब सूर्य आज की तरह ऊर्जा की आपूर्ति नहीं कर सकेगा. हाइड्रोजन की आपूर्ति समाप्त होने पर वह फूलने लगेगा. उस समय सूर्य का आकार आज के आकार की तुलना में ढाई सौ गुना बढ़ जाएगा और इस प्रक्रिया के दौरान सूर्य तब बुध, शुक्र, और पृथ्वी ग्रहों को निगल लेगा. उसके बाद वह सिकुड़ने लगेगा. उस समय सूर्य में मौजूद हीलियम के परमाणु भारी परमाणु में बदलने लगेंगे जिससे ऊर्जा का उत्पादन भी होगा. उस परिस्थिति में सूर्य अंततः इतना छोटा हो जाएगा कि उसकी सारी द्रव्य राशि अंतरिक्ष में पृथ्वी से अधिक स्थान नहीं घेरेगी और अंत में कुछ समय के बाद सूर्य चमकना बंद करके श्वेत तारा बन जाएगा. फिर अनेक वर्षों के बाद श्वेत वामन तारा चमकना बंद कर देगा और अंत में सूर्य एक मृत श्याम वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ पिंड में परिवर्तित हो जाएगा. सूर्य का अस्तित्व लगभग पांच अरब वर्षों से है और अगले दस अरब वर्षों तक इसका अस्तित्व कायम रहेगा.
सूर्य को देखना
अत्यधिक चमक या दीप्ति के कारण सूर्य को नंगी आंखों से देखना खतरनाक हो सकता है इसलिए सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए. इसके अलावा सूर्य को किसी दूरबीन से भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे आंखों को क्षति पहुंचने की संभावना रहती है. किसी अनुभवी खगोलविद् के मार्गदर्शन में विशेष प्रकार के फिल्टर का उपयोग करते हुए सूर्य को देखा जा सकता है.
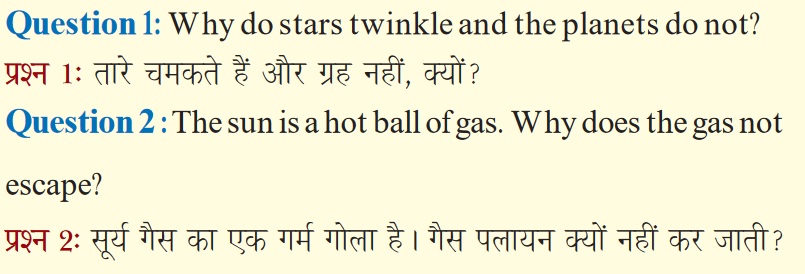
Comments
Post a Comment